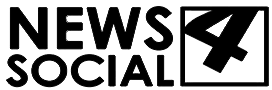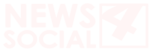पवन के. वर्मा का कॉलम: संसद को कोर्ट के विरोध में खड़ा करना गैरजरूरी टकराव
- Hindi News
- Opinion
- Pawan K. Verma’s Column Pitting Parliament Against The Court Is An Unnecessary Confrontation
2 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
पवन के. वर्मा पूर्व राज्यसभा सांसद व राजनयिक
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक मिलनसार व्यक्ति हैं। कुछ साल पहले मैं कोलकाता में अपनी पुस्तक ‘आदि शंकराचार्य : हिंदू धर्म के महानतम दार्शनिक’ पर बोल रहा था और राज्यपाल के रूप में उन्हें वहां लगभग 15 मिनट के लिए उपस्थित होना था।
लेकिन वे मेरे भाषण के अंत तक रुके। बाद में, जब हम दिल्ली में मिले, तो उन्होंने इस अवसर को जीवंत रूप से याद किया, और बहुत उत्साह से प्रशंसा की। उनके आतिथ्य और तत्पर-विनोद ने मुझ पर एक अलग छाप छोड़ी।
हालांकि, संवैधानिक मामलों में हमारी व्यक्तिगत पसंद-नापसंद गौण होती हैं। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए तो यही ज्यादा मायने रखता है कि वे संविधान की कैसी व्याख्या करते हैं, और इसके भीतर महत्वपूर्ण घटकों की कैसी भूमिका देखते हैं।
उपराष्ट्रपति ने हाल ही में न केवल सर्वोच्च न्यायालय पर ‘न्यायिक अतिक्रमण’ का आरोप लगाया, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 142 को संसद की सर्वोच्चता के खिलाफ ‘परमाणु मिसाइल’ के रूप में इस्तेमाल करने की भी बात कही। ये कठोर शब्द हैं, अलबत्ता उनकी आलोचना-वृत्ति नई नहीं है।
दिसंबर 2022 में पदभार संभालने के तुरंत बाद भी धनखड़ ने ऐतिहासिक केशवानंद भारती फैसले (1973) पर सवाल उठाकर बहस छेड़ दी थी, जिसने संविधान के ‘मूल ढांचे’ की रक्षा के लिए एससी के अधिकार को स्थापित किया था।
उन्होंने इसे संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित करने के रूप में देखा। धनखड़ ने तर्क दिया था कि इस न्यायिक ‘इनोवेशन’ का संविधान में कोई स्पष्ट आधार नहीं था और इसने संसदीय संप्रभुता को कमजोर किया है। तब भी उनकी टिप्पणियों को कई लोगों ने संविधान की व्याख्याता के रूप में न्यायपालिका की भूमिका के लिए एक अप्रत्यक्ष चुनौती की तरह देखा था।
लेकिन उनकी नवीनतम आलोचना, जिसमें उन्होंने राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति के विवेकाधिकार में एससी के हस्तक्षेप पर निशाना साधा है- ने बात को तूल दे दिया है। इसके मूल में राज्यपालों पर एससी की वे टिप्पणियां हैं, जिनमें विशेष रूप से विपक्ष-शासित राज्यों में विधेयकों को दबाए रखने की बात कही गई थी।
तमिलनाडु, केरल और पंजाब में तो राज्य सरकारों ने राज्यपालों पर ‘केंद्र के एजेंट’ के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया, जो वर्षों तक विधेयकों में टालमटोल करते हैं। ऐसे में त्वरित निर्णय लेने पर सर्वोच्च न्यायालय का जोर संवैधानिक कार्यालयों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हथियार बनाने से रोकने के लिए आवश्यक सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए।
लेकिन इस न्यायिक निरीक्षण के प्रति धनखड़ का प्रतिरोध एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। यह कि अगर संवैधानिक पदाधिकारी अपने कर्तव्य में विफल होते हैं, तो जवाबदेही कौन सुनिश्चित करेगा? संविधान स्वयं राज्यपालों या राष्ट्रपति को विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट समयसीमा प्रदान नहीं करता है।
ऐसे परिदृश्य में, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायिक व्याख्या जरूरी हो जाती है। राष्ट्रपति को निर्देश जारी करने का प्रश्न तो हास्यास्पद है, क्योंकि वे एक ऐसे संवैधानिक प्राधिकारी हैं, जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं।
मेरे खयाल से, धनखड़ एक गलत व्याख्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने के लिए संसद के निर्विवाद संवैधानिक अधिकार पर सवाल नहीं उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ यह जांच रहा है कि क्या ऐसे कानून संविधान के अनुरूप हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है। अगर ऐसा न हो तो कोई कार्यपालिका पर कोई रोकटोक नहीं होगी और वह बेलगाम हो सकती है।
उदाहरण के लिए, लोकसभा में पूर्ण बहुमत और राज्यसभा में पर्याप्त संख्याबल की सहायता से कोई राजनीतिक दल भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाला कानून पारित कर सकता है। लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट को इसे रद्द करने का अधिकार होगा, क्योंकि वह कानून संविधान के अनुच्छेद 25 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करने वाला होगा।
अनुच्छेद 25 भारत के सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उसका अभ्यास और प्रचार करने का मौलिक अधिकार देता है, वहीं संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीयों को ‘विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता’ भी प्रदान करता है।
संसद को सुप्रीम कोर्ट के विरोध में खड़ा करके धनखड़ एक अनावश्यक टकराव पैदा कर रहे हैं, जिसे संविधान ने स्पष्ट रूप से शुरू में ही हल कर दिया था। यह संसदीय लोकतंत्र के कामकाज को खतरे में डाल सकता है।
भारत का संविधान स्वयं राज्यपालों या राष्ट्रपति को विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट समयसीमा प्रदान नहीं करता है। ऐसे परिदृश्य में, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायिक व्याख्या और जरूरी हो जाती है।
(ये लेखक के अपने विचार हैं।)
खबरें और भी हैं…
राजनीति की और खबर देखने के लिए यहाँ क्लिक करे – राजनीति
News
- Hindi News
- Opinion
- Pawan K. Verma’s Column Pitting Parliament Against The Court Is An Unnecessary Confrontation
2 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
पवन के. वर्मा पूर्व राज्यसभा सांसद व राजनयिक
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक मिलनसार व्यक्ति हैं। कुछ साल पहले मैं कोलकाता में अपनी पुस्तक ‘आदि शंकराचार्य : हिंदू धर्म के महानतम दार्शनिक’ पर बोल रहा था और राज्यपाल के रूप में उन्हें वहां लगभग 15 मिनट के लिए उपस्थित होना था।
लेकिन वे मेरे भाषण के अंत तक रुके। बाद में, जब हम दिल्ली में मिले, तो उन्होंने इस अवसर को जीवंत रूप से याद किया, और बहुत उत्साह से प्रशंसा की। उनके आतिथ्य और तत्पर-विनोद ने मुझ पर एक अलग छाप छोड़ी।
हालांकि, संवैधानिक मामलों में हमारी व्यक्तिगत पसंद-नापसंद गौण होती हैं। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए तो यही ज्यादा मायने रखता है कि वे संविधान की कैसी व्याख्या करते हैं, और इसके भीतर महत्वपूर्ण घटकों की कैसी भूमिका देखते हैं।
उपराष्ट्रपति ने हाल ही में न केवल सर्वोच्च न्यायालय पर ‘न्यायिक अतिक्रमण’ का आरोप लगाया, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 142 को संसद की सर्वोच्चता के खिलाफ ‘परमाणु मिसाइल’ के रूप में इस्तेमाल करने की भी बात कही। ये कठोर शब्द हैं, अलबत्ता उनकी आलोचना-वृत्ति नई नहीं है।
दिसंबर 2022 में पदभार संभालने के तुरंत बाद भी धनखड़ ने ऐतिहासिक केशवानंद भारती फैसले (1973) पर सवाल उठाकर बहस छेड़ दी थी, जिसने संविधान के ‘मूल ढांचे’ की रक्षा के लिए एससी के अधिकार को स्थापित किया था।
उन्होंने इसे संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित करने के रूप में देखा। धनखड़ ने तर्क दिया था कि इस न्यायिक ‘इनोवेशन’ का संविधान में कोई स्पष्ट आधार नहीं था और इसने संसदीय संप्रभुता को कमजोर किया है। तब भी उनकी टिप्पणियों को कई लोगों ने संविधान की व्याख्याता के रूप में न्यायपालिका की भूमिका के लिए एक अप्रत्यक्ष चुनौती की तरह देखा था।
लेकिन उनकी नवीनतम आलोचना, जिसमें उन्होंने राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति के विवेकाधिकार में एससी के हस्तक्षेप पर निशाना साधा है- ने बात को तूल दे दिया है। इसके मूल में राज्यपालों पर एससी की वे टिप्पणियां हैं, जिनमें विशेष रूप से विपक्ष-शासित राज्यों में विधेयकों को दबाए रखने की बात कही गई थी।
तमिलनाडु, केरल और पंजाब में तो राज्य सरकारों ने राज्यपालों पर ‘केंद्र के एजेंट’ के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया, जो वर्षों तक विधेयकों में टालमटोल करते हैं। ऐसे में त्वरित निर्णय लेने पर सर्वोच्च न्यायालय का जोर संवैधानिक कार्यालयों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हथियार बनाने से रोकने के लिए आवश्यक सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए।
लेकिन इस न्यायिक निरीक्षण के प्रति धनखड़ का प्रतिरोध एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। यह कि अगर संवैधानिक पदाधिकारी अपने कर्तव्य में विफल होते हैं, तो जवाबदेही कौन सुनिश्चित करेगा? संविधान स्वयं राज्यपालों या राष्ट्रपति को विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट समयसीमा प्रदान नहीं करता है।
ऐसे परिदृश्य में, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायिक व्याख्या जरूरी हो जाती है। राष्ट्रपति को निर्देश जारी करने का प्रश्न तो हास्यास्पद है, क्योंकि वे एक ऐसे संवैधानिक प्राधिकारी हैं, जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं।
मेरे खयाल से, धनखड़ एक गलत व्याख्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने के लिए संसद के निर्विवाद संवैधानिक अधिकार पर सवाल नहीं उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ यह जांच रहा है कि क्या ऐसे कानून संविधान के अनुरूप हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है। अगर ऐसा न हो तो कोई कार्यपालिका पर कोई रोकटोक नहीं होगी और वह बेलगाम हो सकती है।
उदाहरण के लिए, लोकसभा में पूर्ण बहुमत और राज्यसभा में पर्याप्त संख्याबल की सहायता से कोई राजनीतिक दल भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाला कानून पारित कर सकता है। लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट को इसे रद्द करने का अधिकार होगा, क्योंकि वह कानून संविधान के अनुच्छेद 25 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करने वाला होगा।
अनुच्छेद 25 भारत के सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उसका अभ्यास और प्रचार करने का मौलिक अधिकार देता है, वहीं संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीयों को ‘विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता’ भी प्रदान करता है।
संसद को सुप्रीम कोर्ट के विरोध में खड़ा करके धनखड़ एक अनावश्यक टकराव पैदा कर रहे हैं, जिसे संविधान ने स्पष्ट रूप से शुरू में ही हल कर दिया था। यह संसदीय लोकतंत्र के कामकाज को खतरे में डाल सकता है।
भारत का संविधान स्वयं राज्यपालों या राष्ट्रपति को विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट समयसीमा प्रदान नहीं करता है। ऐसे परिदृश्य में, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायिक व्याख्या और जरूरी हो जाती है।
(ये लेखक के अपने विचार हैं।)
News