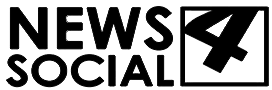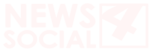संजय कुमार का कॉलम: जातियों को लेकर पूर्वाग्रह अभी तक कम नहीं हुआ है
- Hindi News
- Opinion
- Sanjay Kumar’s Column: Prejudice Regarding Castes Has Not Diminished Yet
6 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
संजय कुमार, प्रोफेसर व राजनीतिक टिप्पणीकार
हाल ही में हमने डॉ. बीआर आम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाई है। इस अवसर पर पूछा गया कि वर्तमान विकसित भारत में डॉ. आम्बेडकर कितने प्रासंगिक हैं। मेरी राय में, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने कि देश की आजादी के शुरुआती वर्षों में थे। और मेरे पास ऐसा कहने के पर्याप्त प्रमाण हैं। मैं इस लेख में इस संबंध में तीन दलीलें पेश करना चाहूंगा।
पहली, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के बावजूद अभी भी दलित और आदिवासी समुदायों के लोगों का ऊंचे पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। दूसरी, जातिगत पूर्वाग्रह अभी भी बहुत मजबूत बने हुए हैं। तीसरी, शिक्षा के व्यापक प्रसार के बावजूद जातिगत पहचान देश में बहुत मजबूत हुई है। पहले की तुलना में एकमात्र बदलाव यह है कि पहले जातिगत पहचान प्रमुख जातियों द्वारा प्रदर्शित की जाती थी, अब यह वर्चस्वशाली जातियों के साथ ही वंचित वर्गों द्वारा भी प्रदर्शित की जाती है।
सबसे पहली बात, आरक्षण के प्रावधानों के बावजूद शैक्षणिक संस्थानों में दलित और आदिवासी समुदायों के लोगों के उच्च पदों (प्राध्यापक), भारतीय नौकरशाही (आईएएस) में शीर्ष ओहदों, केंद्र सरकार की नौकरियों में अच्छी पोजिशन, उच्च न्यायपालिका और अन्य सरकारी नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व के कई सबूत मिलते हैं।
विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में भी यही कहानी है। जहां निचले स्तर पर पदों के लिए रिक्तियों और भरे गए पदों के बीच का अंतर कम हो सकता है, लेकिन उच्च पदों के लिए यह बहुत अधिक है। दलित और आदिवासी समुदायों के लोगों के लिए स्वीकृत पदों पर भर्ती न होने के कई कारण बताए जाते हैं, जिनमें से एक अक्सर उद्धृत किया जाने वाला कारण ‘पद के लिए किसी का भी उपयुक्त नहीं पाया जाना’ है।
आजादी के कई दशक बीतने के बाद भी समाज में जातिगत पूर्वाग्रह बहुत मजबूत बने हुए हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे आस-पड़ोस में, जहां हम रहते हैं और जहां हम काम करते हैं- वहां वंचित जातियों के खिलाफ मजबूत पूर्वाग्रहों की साझा भावना के साक्ष्य मौजूद हैं। कुछ दशक पहले तक दिल्ली में शायद ही कोई पड़ोसी अपने फ्लैट/घर के पास रहने वाले व्यक्ति/परिवार की जाति के बारे में पूछता था, जो कि अब देश की राजधानी में नहीं होता। दबी जुबान से ही सही, लेकिन जाति के बारे में पूछताछ दिल्ली के मध्यम वर्ग के इलाकों में आम बात हो गई है।
इतना ही नहीं, अगर कोई अपना फ्लैट/घर वंचित जातियों के लोगों को किराए पर देने की कोशिश करता है, तो वहां पहले से रह रहा दूसरा पड़ोसी विनम्रता से कह सकता है कि कृपया किसी ‘अच्छे परिवार’ को किराए पर दें। स्पष्ट संदेश यह है कि एक प्रभावशाली जाति से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति किसी वंचित वर्ग के व्यक्ति को फ्लैट भी किराए पर नहीं दे सकता।
शहरी भारत में लोग आज ‘कुमार’ जैसे अस्पष्ट उपनाम वाले या बिना उपनाम वाले व्यक्तियों की जाति जानने के लिए पहले से कहीं ज्यादा उत्सुक हो गए हैं। राष्ट्रीय प्रतिनिधि सैम्पल के साथ बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के साक्ष्य भी भारत में निचली जातियों के खिलाफ पूर्वाग्रह की एक मजबूत भावना का संकेत देते हैं।
एक तिहाई भारतीयों का मानना है कि दलित और आदिवासी अभी तक मुख्यधारा के अन्य वर्गों के बराबर नहीं आ पाए हैं, क्योंकि वे इसके लिए प्रयास नहीं करते हैं। या कि वे कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, जो मानते हैं कि इसका कारण मेहनत की कमी नहीं बल्कि अवसरों से वंचित होना है। सर्वेक्षण में दलित और आदिवासी समुदायों से वास्ता रखने वाले कई युवाओं ने दैनिक जीवन में भेदभाव का सामना करना स्वीकार किया।
ऐसे लोग भी हैं, जो त्वचा के रंग, आर्थिक वर्ग, क्षेत्र, अंग्रेजी बोलने की अक्षमता आदि के कारण भेदभाव का सामना करते हैं। लेकिन निचली जाति से संबंधित होने के कारण भेदभाव का सामना करना आज भी इनसे अधिक प्रचलित है। इसकी तुलना किसी विशेष धर्म से संबंधित होने के कारण होने वाले भेदभाव से ही की जा सकती है।
यह भी माना जाता है कि पुलिस, न्यायपालिका और नौकरशाही निचली जातियों की तुलना में उच्च जातियों को तरजीह देती है। यह धारणा वंचित जातियों के रोजमर्रा के अनुभवों पर आधरित है। इतना ही नहीं, समाज के विभिन्न वर्गों में शिक्षा के प्रसार के बावजूद जातिगत पहचान भी पहले की तुलना में अब बहुत मजबूत हो गई है। यह समूचा परिदृश्य डॉ. आम्बेडकर को आज भी प्रासंगिक बनाता है।
- आरक्षण के बावजूद शैक्षणिक संस्थानों में वंचित वर्ग के लोगों के उच्च पदों (प्राध्यापक), नौकरशाही (आईएएस) में शीर्ष ओहदों, सरकारी नौकरियों में अच्छी पोजिशन, उच्च न्यायपालिका में कम प्रतिनिधित्व के कई सबूत मिलते हैं।
(ये लेखक के अपने विचार हैं।)
खबरें और भी हैं…
राजनीति की और खबर देखने के लिए यहाँ क्लिक करे – राजनीति
News
- Hindi News
- Opinion
- Sanjay Kumar’s Column: Prejudice Regarding Castes Has Not Diminished Yet
6 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
संजय कुमार, प्रोफेसर व राजनीतिक टिप्पणीकार
हाल ही में हमने डॉ. बीआर आम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाई है। इस अवसर पर पूछा गया कि वर्तमान विकसित भारत में डॉ. आम्बेडकर कितने प्रासंगिक हैं। मेरी राय में, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने कि देश की आजादी के शुरुआती वर्षों में थे। और मेरे पास ऐसा कहने के पर्याप्त प्रमाण हैं। मैं इस लेख में इस संबंध में तीन दलीलें पेश करना चाहूंगा।
पहली, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के बावजूद अभी भी दलित और आदिवासी समुदायों के लोगों का ऊंचे पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। दूसरी, जातिगत पूर्वाग्रह अभी भी बहुत मजबूत बने हुए हैं। तीसरी, शिक्षा के व्यापक प्रसार के बावजूद जातिगत पहचान देश में बहुत मजबूत हुई है। पहले की तुलना में एकमात्र बदलाव यह है कि पहले जातिगत पहचान प्रमुख जातियों द्वारा प्रदर्शित की जाती थी, अब यह वर्चस्वशाली जातियों के साथ ही वंचित वर्गों द्वारा भी प्रदर्शित की जाती है।
सबसे पहली बात, आरक्षण के प्रावधानों के बावजूद शैक्षणिक संस्थानों में दलित और आदिवासी समुदायों के लोगों के उच्च पदों (प्राध्यापक), भारतीय नौकरशाही (आईएएस) में शीर्ष ओहदों, केंद्र सरकार की नौकरियों में अच्छी पोजिशन, उच्च न्यायपालिका और अन्य सरकारी नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व के कई सबूत मिलते हैं।
विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में भी यही कहानी है। जहां निचले स्तर पर पदों के लिए रिक्तियों और भरे गए पदों के बीच का अंतर कम हो सकता है, लेकिन उच्च पदों के लिए यह बहुत अधिक है। दलित और आदिवासी समुदायों के लोगों के लिए स्वीकृत पदों पर भर्ती न होने के कई कारण बताए जाते हैं, जिनमें से एक अक्सर उद्धृत किया जाने वाला कारण ‘पद के लिए किसी का भी उपयुक्त नहीं पाया जाना’ है।
आजादी के कई दशक बीतने के बाद भी समाज में जातिगत पूर्वाग्रह बहुत मजबूत बने हुए हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे आस-पड़ोस में, जहां हम रहते हैं और जहां हम काम करते हैं- वहां वंचित जातियों के खिलाफ मजबूत पूर्वाग्रहों की साझा भावना के साक्ष्य मौजूद हैं। कुछ दशक पहले तक दिल्ली में शायद ही कोई पड़ोसी अपने फ्लैट/घर के पास रहने वाले व्यक्ति/परिवार की जाति के बारे में पूछता था, जो कि अब देश की राजधानी में नहीं होता। दबी जुबान से ही सही, लेकिन जाति के बारे में पूछताछ दिल्ली के मध्यम वर्ग के इलाकों में आम बात हो गई है।
इतना ही नहीं, अगर कोई अपना फ्लैट/घर वंचित जातियों के लोगों को किराए पर देने की कोशिश करता है, तो वहां पहले से रह रहा दूसरा पड़ोसी विनम्रता से कह सकता है कि कृपया किसी ‘अच्छे परिवार’ को किराए पर दें। स्पष्ट संदेश यह है कि एक प्रभावशाली जाति से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति किसी वंचित वर्ग के व्यक्ति को फ्लैट भी किराए पर नहीं दे सकता।
शहरी भारत में लोग आज ‘कुमार’ जैसे अस्पष्ट उपनाम वाले या बिना उपनाम वाले व्यक्तियों की जाति जानने के लिए पहले से कहीं ज्यादा उत्सुक हो गए हैं। राष्ट्रीय प्रतिनिधि सैम्पल के साथ बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के साक्ष्य भी भारत में निचली जातियों के खिलाफ पूर्वाग्रह की एक मजबूत भावना का संकेत देते हैं।
एक तिहाई भारतीयों का मानना है कि दलित और आदिवासी अभी तक मुख्यधारा के अन्य वर्गों के बराबर नहीं आ पाए हैं, क्योंकि वे इसके लिए प्रयास नहीं करते हैं। या कि वे कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, जो मानते हैं कि इसका कारण मेहनत की कमी नहीं बल्कि अवसरों से वंचित होना है। सर्वेक्षण में दलित और आदिवासी समुदायों से वास्ता रखने वाले कई युवाओं ने दैनिक जीवन में भेदभाव का सामना करना स्वीकार किया।
ऐसे लोग भी हैं, जो त्वचा के रंग, आर्थिक वर्ग, क्षेत्र, अंग्रेजी बोलने की अक्षमता आदि के कारण भेदभाव का सामना करते हैं। लेकिन निचली जाति से संबंधित होने के कारण भेदभाव का सामना करना आज भी इनसे अधिक प्रचलित है। इसकी तुलना किसी विशेष धर्म से संबंधित होने के कारण होने वाले भेदभाव से ही की जा सकती है।
यह भी माना जाता है कि पुलिस, न्यायपालिका और नौकरशाही निचली जातियों की तुलना में उच्च जातियों को तरजीह देती है। यह धारणा वंचित जातियों के रोजमर्रा के अनुभवों पर आधरित है। इतना ही नहीं, समाज के विभिन्न वर्गों में शिक्षा के प्रसार के बावजूद जातिगत पहचान भी पहले की तुलना में अब बहुत मजबूत हो गई है। यह समूचा परिदृश्य डॉ. आम्बेडकर को आज भी प्रासंगिक बनाता है।
- आरक्षण के बावजूद शैक्षणिक संस्थानों में वंचित वर्ग के लोगों के उच्च पदों (प्राध्यापक), नौकरशाही (आईएएस) में शीर्ष ओहदों, सरकारी नौकरियों में अच्छी पोजिशन, उच्च न्यायपालिका में कम प्रतिनिधित्व के कई सबूत मिलते हैं।
(ये लेखक के अपने विचार हैं।)
News