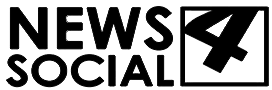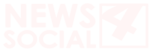शक्ति के विकेंद्रिकरण को ध्यान में रखकर ग्राम पंचायत की अवधारणा का विकास हुआ. हर गाँव की एक पंचायत होती है. उस गाँव के लोग अपने में से ही पंच और सरपंच का चुनाव करते हैं. जिनका काम गाँव स्तर पर प्रशासन को देखना होता है. गाँव को कई वार्डो में विभाजित किया जाता है. जिसमें से एक-एक पंच का चुनाव होता है. गाँव में ग्राम पंचायत एक कार्यपालन और निर्वाचित संस्था है.
लेकिन यदि किसी भी कारण से गाँव की पंचायत को भंग किया जाता है, तो उसके बाद दोबारा चुनाव कराए जाते हैं. ताकि गाँव के स्तर पर विकास कार्यों में कोई अवरोध पैदा ना हो. अगर चुनाव होते हैं, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा 6 महिनें का समय निर्धारित किया जाता है. पंचायत भंग होने के 6 महिनें के अंदर-अंदर दोबारा पंचायत चुनाव कराने जरूरी होते हैं.
1947 ई. तक ग्रामों में सही पंचायत व्यवस्था का अभाव ही रहा. देश के आजाद होने के बाद पंचायत व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के सक्रिय प्रयास शुरू हुए. उत्तर प्रदेश में सन् 1947 में पंचायत राज अधिनियम बनाया गया. भारतीय संविधान के अंतर्गत “राजनीति के निदेशक तत्वों” में राज्य का यह प्रमुख कर्तव्य बतलाया गया कि “वह ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर हो” तथा “उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करे जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों”. इस निर्देश के अनुसार प्रत्येक राज्य में पंचायत व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम उठाए गए और प्रत्येक ग्राम अथवा ग्रामसमूह में पंचायत की स्थापना की गई.
यह भी पढ़ें: सिक्किम में पहली सरकार किस पार्टी की बनी और कब
ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष को होता है. आमतौर पर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं. जिसमें पंच और सरपंचो का चुनाव गाँव के मताधिकार प्राप्त लोगों द्वारा किया जाता है.