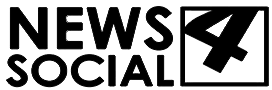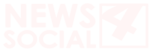अर्घ्य सेनगुप्ता और जय ओझा का कॉलम: हमारे देश में संविधान पर तीन प्रकार के दृष्टिकोण मौजूद हैं
- Hindi News
- Opinion
- Column By Arghya Sengupta And Jai Ojha There Are Three Types Of Views On The Constitution In Our Country
15 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
अर्घ्य सेनगुप्ता और जय ओझा विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के संस्थापक और रिसर्च फेलो
अगर देश की जनता पूछना चाहे कि संसद के शीतकालीन सत्र में क्या कामकाज हुआ तो इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उत्तर संतोषजनक नहीं होगा। सत्र में दोनों सदनों द्वारा केवल एक विधेयक पारित किया गया।
विमान अधिनियम, 1934 को भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 के रूप में पुनः लागू भर किया गया। जबकि पिछले तीन शीतकालीन सत्रों में औसतन 9 विधेयक पारित हुए थे। इस सत्र में वही पैटर्न दोहराया गया, जिसके हम आदी हो चुके हैं : विरोध-प्रदर्शन, फब्तियां और बार-बार स्थगन।
लेकिन इससे पहले संसद में हुई उच्च गुणवत्तापूर्ण बहस को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चार दिनों तक दोनों सदनों ने ‘भारत के संविधान की 75 साल की यात्रा’ पर चर्चा की। सभी पक्षों ने संविधान पर अपना दावा पेश किया- कांग्रेस ने इसके संस्थापक के रूप में और भाजपा ने इसके उत्तराधिकारी के रूप में। हालांकि बारीकी से देखें तो उस बहस ने संविधान पर तीन अलग-अलग दृष्टिकोणों को उजागर किया, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद हमारे गणतंत्र को आकार दिया है।
पहला दृष्टिकोण वह है, जिसे हम ‘नेहरू का संविधान’ कह सकते हैं। नेहरू ने संविधान को एक समानतापूर्ण समाज प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा था। उदाहरण के लिए, ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ के बचाव में 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में अपने भाषण में नेहरू ने तर्क दिया कि जिस वास्तविक स्वतंत्रता के लिए हमने आवाज उठाई है, उसका उद्देश्य हमारे भूखे लोगों को भोजन, कपड़े, आवास और प्रगति के सभी प्रकार के अवसर प्रदान करना था।
आर्थिक विषमता, डिजिटल विभाजन और ‘भाईचारे’ के संवैधानिक मूल्य के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए कपिल सिब्बल ने संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में अपने भाषण में इसी भावना को प्रदर्शित किया।
अपने प्रधानमंत्री काल के दौरान असमानताओं को खत्म करने की नेहरू की इच्छा कभी-कभी उन्हें पारम्परिक संवैधानिक स्वतंत्रताओं को दरकिनार करने के लिए भी प्रेरित कर देती थी। उदाहरण के लिए, 1954 में नेहरू ने खुद संविधान (चौथा संशोधन) विधेयक पेश किया, ताकि संपत्ति के अधिकार को कम किया जा सके, जो तब भी एक मौलिक अधिकार था।
तब डॉ. आम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों के साथ अवमानना करने के इस रवैये पर व्यंग्य करते हुए विरोध जताया था। उन्होंने निजी संपत्ति के अधिकार और मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ के खतरों के बारे में ऐसे शब्दों में बचाव किया, जो उदार मूल्यों के किसी भी समर्थक के लिए जाने-पहचाने होंगे।
डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने संविधान पर बहस में अपने योगदान में नेहरू के समाजवादी के बजाय आम्बेडकर के उदारवादी विचारों को शामिल किया। अपने भाषण में सिंघवी ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह लोकतंत्र का चोला पहनकर तानाशाही कर रही है।
उन्होंने ‘बुलडोजर राज’ के अन्याय, राज्यपाल पद के दुरुपयोग और संघीय ढांचे की अवहेलना की ओर ध्यान खींचा। ये मुद्दे इस बात के मूल में जाते हैं कि एक ऐसे देश में रहना क्या मायने रखता है जो कानूनों द्वारा शासित है, न कि मनुष्यों द्वारा। जहां ‘नेहरूवादी’ संविधान सरकार को अन्याय का इलाज करने के लिए सशक्त करेगा, वहीं ‘आम्बेडकरवादी’ संविधान उसके आवेगों पर अंकुश लगाने की भरसक कोशिश करेगा।
बहस के दौरान एक तीसरा दृष्टिकोण भी उभरा। इसके अनुसार, हमारा संविधान न तो नेहरू का है और न ही आम्बेडकर का, बल्कि यह ‘भारत का संविधान’ है। इस दृष्टिकोण को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में विस्तार से बताया। सिंह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्धृत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि संविधान सामूहिक सहमति का परिणाम है।
उन्होंने 1944 में हिंदू महासभा द्वारा अनुमोदित हिंदुस्थान स्वतंत्र राष्ट्र के संविधान की ओर इशारा किया। संविधान के उस मसौदे में व्यक्तिगत अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद की भी गारंटी दी गई थी। यह दृष्टिकोण देश में संवैधानिक मूल्यों की गहरी जड़ों की ओर इशारा करता है। यह एक ऐसी संस्कृति का स्वाभाविक परिणाम है, जो विविधताओं और मतभेदों का सम्मान करती है।
संविधान के इन तीन दृष्टिकोणों में से किसी को भी ‘गलत’ नहीं बताया जा सकता। बल्कि वे मौलिक प्रश्नों के प्रति भिन्न नजरियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह आवश्यक है कि उन्हें जीवंत बहस में पेश किया जाए। दु:ख की बात है कि ऐसी सार्थक बहस शीतकालीन सत्र की बचकानी जुबानी जंग में समाप्त हो गई।
‘नेहरूवादी’ संविधान सरकार को अन्याय का इलाज करने के लिए सशक्त करेगा, वहीं ‘आम्बेडकरवादी’ संविधान उसके आवेगों पर अंकुश लगाने की कोशिश करेगा। लेकिन ‘भारत का संविधान’ सामूहिक सहमति का परिणाम है। (ये लेखकों के अपने विचार हैं।)
खबरें और भी हैं…
राजनीति की और खबर देखने के लिए यहाँ क्लिक करे – राजनीति
News
- Hindi News
- Opinion
- Column By Arghya Sengupta And Jai Ojha There Are Three Types Of Views On The Constitution In Our Country
15 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
अर्घ्य सेनगुप्ता और जय ओझा विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के संस्थापक और रिसर्च फेलो
अगर देश की जनता पूछना चाहे कि संसद के शीतकालीन सत्र में क्या कामकाज हुआ तो इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उत्तर संतोषजनक नहीं होगा। सत्र में दोनों सदनों द्वारा केवल एक विधेयक पारित किया गया।
विमान अधिनियम, 1934 को भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 के रूप में पुनः लागू भर किया गया। जबकि पिछले तीन शीतकालीन सत्रों में औसतन 9 विधेयक पारित हुए थे। इस सत्र में वही पैटर्न दोहराया गया, जिसके हम आदी हो चुके हैं : विरोध-प्रदर्शन, फब्तियां और बार-बार स्थगन।
लेकिन इससे पहले संसद में हुई उच्च गुणवत्तापूर्ण बहस को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चार दिनों तक दोनों सदनों ने ‘भारत के संविधान की 75 साल की यात्रा’ पर चर्चा की। सभी पक्षों ने संविधान पर अपना दावा पेश किया- कांग्रेस ने इसके संस्थापक के रूप में और भाजपा ने इसके उत्तराधिकारी के रूप में। हालांकि बारीकी से देखें तो उस बहस ने संविधान पर तीन अलग-अलग दृष्टिकोणों को उजागर किया, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद हमारे गणतंत्र को आकार दिया है।
पहला दृष्टिकोण वह है, जिसे हम ‘नेहरू का संविधान’ कह सकते हैं। नेहरू ने संविधान को एक समानतापूर्ण समाज प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा था। उदाहरण के लिए, ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ के बचाव में 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में अपने भाषण में नेहरू ने तर्क दिया कि जिस वास्तविक स्वतंत्रता के लिए हमने आवाज उठाई है, उसका उद्देश्य हमारे भूखे लोगों को भोजन, कपड़े, आवास और प्रगति के सभी प्रकार के अवसर प्रदान करना था।
आर्थिक विषमता, डिजिटल विभाजन और ‘भाईचारे’ के संवैधानिक मूल्य के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए कपिल सिब्बल ने संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में अपने भाषण में इसी भावना को प्रदर्शित किया।
अपने प्रधानमंत्री काल के दौरान असमानताओं को खत्म करने की नेहरू की इच्छा कभी-कभी उन्हें पारम्परिक संवैधानिक स्वतंत्रताओं को दरकिनार करने के लिए भी प्रेरित कर देती थी। उदाहरण के लिए, 1954 में नेहरू ने खुद संविधान (चौथा संशोधन) विधेयक पेश किया, ताकि संपत्ति के अधिकार को कम किया जा सके, जो तब भी एक मौलिक अधिकार था।
तब डॉ. आम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों के साथ अवमानना करने के इस रवैये पर व्यंग्य करते हुए विरोध जताया था। उन्होंने निजी संपत्ति के अधिकार और मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ के खतरों के बारे में ऐसे शब्दों में बचाव किया, जो उदार मूल्यों के किसी भी समर्थक के लिए जाने-पहचाने होंगे।
डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने संविधान पर बहस में अपने योगदान में नेहरू के समाजवादी के बजाय आम्बेडकर के उदारवादी विचारों को शामिल किया। अपने भाषण में सिंघवी ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह लोकतंत्र का चोला पहनकर तानाशाही कर रही है।
उन्होंने ‘बुलडोजर राज’ के अन्याय, राज्यपाल पद के दुरुपयोग और संघीय ढांचे की अवहेलना की ओर ध्यान खींचा। ये मुद्दे इस बात के मूल में जाते हैं कि एक ऐसे देश में रहना क्या मायने रखता है जो कानूनों द्वारा शासित है, न कि मनुष्यों द्वारा। जहां ‘नेहरूवादी’ संविधान सरकार को अन्याय का इलाज करने के लिए सशक्त करेगा, वहीं ‘आम्बेडकरवादी’ संविधान उसके आवेगों पर अंकुश लगाने की भरसक कोशिश करेगा।
बहस के दौरान एक तीसरा दृष्टिकोण भी उभरा। इसके अनुसार, हमारा संविधान न तो नेहरू का है और न ही आम्बेडकर का, बल्कि यह ‘भारत का संविधान’ है। इस दृष्टिकोण को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में विस्तार से बताया। सिंह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्धृत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि संविधान सामूहिक सहमति का परिणाम है।
उन्होंने 1944 में हिंदू महासभा द्वारा अनुमोदित हिंदुस्थान स्वतंत्र राष्ट्र के संविधान की ओर इशारा किया। संविधान के उस मसौदे में व्यक्तिगत अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद की भी गारंटी दी गई थी। यह दृष्टिकोण देश में संवैधानिक मूल्यों की गहरी जड़ों की ओर इशारा करता है। यह एक ऐसी संस्कृति का स्वाभाविक परिणाम है, जो विविधताओं और मतभेदों का सम्मान करती है।
संविधान के इन तीन दृष्टिकोणों में से किसी को भी ‘गलत’ नहीं बताया जा सकता। बल्कि वे मौलिक प्रश्नों के प्रति भिन्न नजरियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह आवश्यक है कि उन्हें जीवंत बहस में पेश किया जाए। दु:ख की बात है कि ऐसी सार्थक बहस शीतकालीन सत्र की बचकानी जुबानी जंग में समाप्त हो गई।
‘नेहरूवादी’ संविधान सरकार को अन्याय का इलाज करने के लिए सशक्त करेगा, वहीं ‘आम्बेडकरवादी’ संविधान उसके आवेगों पर अंकुश लगाने की कोशिश करेगा। लेकिन ‘भारत का संविधान’ सामूहिक सहमति का परिणाम है। (ये लेखकों के अपने विचार हैं।)
News