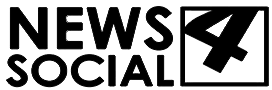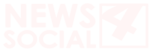पुरानी पेंशन स्कीम : अपने बुजुर्गों को बाजार के भरोसे कैसे छोड़ दें
आनंद प्रधान
राजस्थान के मुख्यमंत्री और साथ में वित्त मंत्री का पदभार संभाल रहे अशोक गहलोत ने बीते सप्ताह विधानसभा में अगले वित्तीय वर्ष का बजट पेश करते हुए 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने का एलान करके एक तरह से बर्र के छत्ते को छेड़ दिया है। राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस एलान को ‘मास्टरस्ट्रोक’ माना जा रहा है, क्योंकि हिंदी पट्टी के बाकी राज्यों की तरह राजस्थान की राजनीति में भी प्रदेश के लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारी निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
ओपीएस का जिन्न
राजस्थान में कांग्रेस सरकार के इस फैसले ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के माहौल को भी गर्म कर दिया है। यूपी में 12 लाख से ज्यादा कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था (ओपीएस) बहाल करने के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ-साथ बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने भी ने सरकार बनने पर ओपीएस बहाल करने का वायदा किया है। जल्दी ही अन्य राज्यों और राजनीतिक दलों में इसे लपकने की होड़ लग सकती है। साफ है कि देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 से पहले लागू पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग का जिन्न फिर से जिंदा हो गया है। लेकिन इसके साथ ही इस मांग और राजस्थान सरकार के फैसले के आर्थिक-वित्तीय औचित्य पर भी सवाल उठाए जाने लगे हैं।

पुरानी पेंशन व्यवस्था के आलोचकों का मुख्य तर्क यह है कि इसे लागू करने से राज्य सरकारों के खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा, जिससे उनके दिवालिया होने का खतरा बढ़ जाएगा। उनके मुताबिक, यह फैसला आर्थिक-वित्तीय दुर्घटना या बर्बादी को निमंत्रण है क्योंकि पहले ही ज्यादातर राज्य सरकारों के बजट का बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में ही खर्च हो जाता है। ऐसे में, ओपीएस लागू करने के बाद उनके लिए विकास और सामाजिक सुरक्षा के दूसरे मदों पर खर्च के लिए पैसा नहीं बचेगा। ओपीएस के आलोचकों के मुताबिक, पुरानी पेंशन की जगह पर लागू नई/राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था (एनपीएस) न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और पेंशन की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त है बल्कि ज्यादा व्यावहारिक और सरकारी खजाने के अनुकूल है।
सरकारी कर्मचारियों का बड़ा हिस्सा इन तर्कों और आलोचनाओं से सहमत नहीं है। उनका तर्क है कि रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन के लिए सरकारी खजाने से निश्चित पेंशन उनका अधिकार है। लेकिन नई/राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था कर्मचारियों के योगदान पर आधारित (डिफाइंड कंट्रीब्यूशन-डीसी) व्यवस्था है जिसमें उनके वेतन और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी और सरकार की ओर से 14 फीसदी का योगदान किया जाता है। इस रकम को बाजार खासकर शेयर बाजार और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है जिसे सरकार की ओर से नियुक्त फंड मैनेजर संभालते हैं। इस व्यवस्था में पेंशन फंड में जमा कुल धनराशि और उस पर मिले रिटर्न से ही कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी।
इस तरह एनपीएस में पेंशन की राशि कर्मचारियों के सेवाकाल की अवधि और उनके योगदान के साथ-साथ बाजार की परिस्थितियों और अपेक्षित रिटर्न पर निर्भर है, जिसमें जाहिर है कि कोई निश्चितता नहीं है। वह बाजार के हाल और उतार-चढ़ाव पर निर्भर है। लेकिन पुरानी पेंशन व्यवस्था पहले से निश्चित लाभ (डिफाइंड बेनिफिट-डीबी) आधारित पेंशन व्यवस्था है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सरकारी खजाने से उनके अंतिम वेतन का 50 फीसदी तक निश्चित पेंशन मिलती है। इसमें हर छह महीने पर महंगाई भत्ते की वृद्धि भी शामिल की जाती है।
दरअसल, यह एक-दूसरे से अलग दो पेंशन व्यवस्थाओं का ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी दो आर्थिक नीतियों और दृष्टियों का भी टकराव है जिसमें एक ओर कल्याणकारी राज्य के दौर में शुरू की गई पूर्व निश्चित लाभ पर आधारित पुरानी पेंशन व्यवस्था है, और दूसरी ओर नव उदारवादी आर्थिक सैद्धांतिकी के दौर में आर्थिक सुधारों के तहत शुरू की गई योगदान पर आधारित नई/राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था है, जिसमें राज्य ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और सब कुछ बाजार भरोसे है।
यह सच है कि पिछले कुछ दशकों में नव उदारवादी आर्थिक सुधारों के तहत ज्यादातर देशों में भारत की एनपीएस जैसी पेंशन व्यवस्था को ही आगे बढ़ाया गया है। लेकिन नव उदारवादी आर्थिक सुधारों के बीच तेजी से बढ़ती गैर-बराबरी और कमजोर होती सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के कारण हाल के वर्षों में दुनिया के बहुतेरे देशों में ओपीएस जैसी पूर्व निश्चित लाभ पर आधारित पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है।
असल में, पेंशन का मुद्दा व्यापक सामाजिक सुरक्षा और उसे सुनिश्चित करने में राज्य की भूमिका से जुड़ा सवाल है। इसे सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के विशेषाधिकार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद गरिमापूर्ण जीवन के लिए पेंशन जैसे जरूरी सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे को सिर्फ वित्तीय व्यवहारिकता के आधार पर देखना नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। सचाई यह है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और कल्याणकारी दृष्टि हो तो वित्तीय संसाधन भी आसानी से जुट जाते हैं।
मनरेगा है मिसाल
याद दिलाने की जरूरत नहीं कि जब मनरेगा, मिड-डे मील और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं शुरू की गई थीं, तब भी यह तर्क दिया गया था कि इससे सरकारी खजाने का दिवाला निकल जाएगा या अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। न सिर्फ इन योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने में कोई परेशानी नहीं हुई बल्कि ये योजनाएं अपने सामाजिक उद्देश्यों को भी पूरा करने में कामयाब रही हैं। वास्तव में, आज देश में सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के वास्ते पूर्व निश्चित लाभ पर आधारित एक राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था शुरू करने पर गंभीरता से विचार करने का वक्त आ गया है। दुनिया भर में पिछले कुछ समय से यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जरूरत पर चर्चा यूं ही जोर नहीं पकड़ रही है।
आनंद प्रधान
राजस्थान के मुख्यमंत्री और साथ में वित्त मंत्री का पदभार संभाल रहे अशोक गहलोत ने बीते सप्ताह विधानसभा में अगले वित्तीय वर्ष का बजट पेश करते हुए 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने का एलान करके एक तरह से बर्र के छत्ते को छेड़ दिया है। राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस एलान को ‘मास्टरस्ट्रोक’ माना जा रहा है, क्योंकि हिंदी पट्टी के बाकी राज्यों की तरह राजस्थान की राजनीति में भी प्रदेश के लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारी निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
ओपीएस का जिन्न
राजस्थान में कांग्रेस सरकार के इस फैसले ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के माहौल को भी गर्म कर दिया है। यूपी में 12 लाख से ज्यादा कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था (ओपीएस) बहाल करने के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ-साथ बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने भी ने सरकार बनने पर ओपीएस बहाल करने का वायदा किया है। जल्दी ही अन्य राज्यों और राजनीतिक दलों में इसे लपकने की होड़ लग सकती है। साफ है कि देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 से पहले लागू पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग का जिन्न फिर से जिंदा हो गया है। लेकिन इसके साथ ही इस मांग और राजस्थान सरकार के फैसले के आर्थिक-वित्तीय औचित्य पर भी सवाल उठाए जाने लगे हैं।
पुरानी पेंशन व्यवस्था के आलोचकों का मुख्य तर्क यह है कि इसे लागू करने से राज्य सरकारों के खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा, जिससे उनके दिवालिया होने का खतरा बढ़ जाएगा। उनके मुताबिक, यह फैसला आर्थिक-वित्तीय दुर्घटना या बर्बादी को निमंत्रण है क्योंकि पहले ही ज्यादातर राज्य सरकारों के बजट का बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में ही खर्च हो जाता है। ऐसे में, ओपीएस लागू करने के बाद उनके लिए विकास और सामाजिक सुरक्षा के दूसरे मदों पर खर्च के लिए पैसा नहीं बचेगा। ओपीएस के आलोचकों के मुताबिक, पुरानी पेंशन की जगह पर लागू नई/राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था (एनपीएस) न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और पेंशन की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त है बल्कि ज्यादा व्यावहारिक और सरकारी खजाने के अनुकूल है।
सरकारी कर्मचारियों का बड़ा हिस्सा इन तर्कों और आलोचनाओं से सहमत नहीं है। उनका तर्क है कि रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन के लिए सरकारी खजाने से निश्चित पेंशन उनका अधिकार है। लेकिन नई/राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था कर्मचारियों के योगदान पर आधारित (डिफाइंड कंट्रीब्यूशन-डीसी) व्यवस्था है जिसमें उनके वेतन और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी और सरकार की ओर से 14 फीसदी का योगदान किया जाता है। इस रकम को बाजार खासकर शेयर बाजार और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है जिसे सरकार की ओर से नियुक्त फंड मैनेजर संभालते हैं। इस व्यवस्था में पेंशन फंड में जमा कुल धनराशि और उस पर मिले रिटर्न से ही कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी।
इस तरह एनपीएस में पेंशन की राशि कर्मचारियों के सेवाकाल की अवधि और उनके योगदान के साथ-साथ बाजार की परिस्थितियों और अपेक्षित रिटर्न पर निर्भर है, जिसमें जाहिर है कि कोई निश्चितता नहीं है। वह बाजार के हाल और उतार-चढ़ाव पर निर्भर है। लेकिन पुरानी पेंशन व्यवस्था पहले से निश्चित लाभ (डिफाइंड बेनिफिट-डीबी) आधारित पेंशन व्यवस्था है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सरकारी खजाने से उनके अंतिम वेतन का 50 फीसदी तक निश्चित पेंशन मिलती है। इसमें हर छह महीने पर महंगाई भत्ते की वृद्धि भी शामिल की जाती है।
दरअसल, यह एक-दूसरे से अलग दो पेंशन व्यवस्थाओं का ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी दो आर्थिक नीतियों और दृष्टियों का भी टकराव है जिसमें एक ओर कल्याणकारी राज्य के दौर में शुरू की गई पूर्व निश्चित लाभ पर आधारित पुरानी पेंशन व्यवस्था है, और दूसरी ओर नव उदारवादी आर्थिक सैद्धांतिकी के दौर में आर्थिक सुधारों के तहत शुरू की गई योगदान पर आधारित नई/राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था है, जिसमें राज्य ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और सब कुछ बाजार भरोसे है।
यह सच है कि पिछले कुछ दशकों में नव उदारवादी आर्थिक सुधारों के तहत ज्यादातर देशों में भारत की एनपीएस जैसी पेंशन व्यवस्था को ही आगे बढ़ाया गया है। लेकिन नव उदारवादी आर्थिक सुधारों के बीच तेजी से बढ़ती गैर-बराबरी और कमजोर होती सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के कारण हाल के वर्षों में दुनिया के बहुतेरे देशों में ओपीएस जैसी पूर्व निश्चित लाभ पर आधारित पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है।
असल में, पेंशन का मुद्दा व्यापक सामाजिक सुरक्षा और उसे सुनिश्चित करने में राज्य की भूमिका से जुड़ा सवाल है। इसे सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के विशेषाधिकार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद गरिमापूर्ण जीवन के लिए पेंशन जैसे जरूरी सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे को सिर्फ वित्तीय व्यवहारिकता के आधार पर देखना नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। सचाई यह है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और कल्याणकारी दृष्टि हो तो वित्तीय संसाधन भी आसानी से जुट जाते हैं।
मनरेगा है मिसाल
याद दिलाने की जरूरत नहीं कि जब मनरेगा, मिड-डे मील और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं शुरू की गई थीं, तब भी यह तर्क दिया गया था कि इससे सरकारी खजाने का दिवाला निकल जाएगा या अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। न सिर्फ इन योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने में कोई परेशानी नहीं हुई बल्कि ये योजनाएं अपने सामाजिक उद्देश्यों को भी पूरा करने में कामयाब रही हैं। वास्तव में, आज देश में सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के वास्ते पूर्व निश्चित लाभ पर आधारित एक राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था शुरू करने पर गंभीरता से विचार करने का वक्त आ गया है। दुनिया भर में पिछले कुछ समय से यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जरूरत पर चर्चा यूं ही जोर नहीं पकड़ रही है।
डिसक्लेमर : ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं