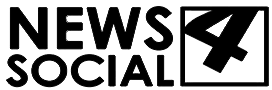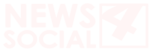शेखर गुप्ता का कॉलम: रुपहले परदे पर कैसे बदले राष्ट्रवाद के रूप
- Hindi News
- Opinion
- Shekhar Gupta’s Column How The Form Of Nationalism Changed On The Silver Screen
28 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
शेखर गुप्ता, एडिटर-इन-चीफ, ‘द प्रिन्ट’
पिछले छह दशकों में राष्ट्रभक्ति का विकास किस तरह हुआ, इसे समझने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि हम देखें भारतीय सिनेमा और खासकर बॉलीवुड ने अलग-अलग दौर में इसे कैसे परिभाषित किया। मनोज कुमार की मृत्यु हमें इस बात पर विचार करने का मौका देती है।
देशभक्ति, राष्ट्रवाद, नागरिक-बोध, अनुशासित जीवनशैली आदि सबको उन्होंने जितना परिभाषित किया, उतना किसी दूसरे अभिनेता ने शायद ही किया होगा। अपने पसंदीदा नाम ‘भारत’ के रूप में वे तरह-तरह के किरदारों को फिल्मी परदे पर जीते हुए एक मुकम्मल भारतीय के चरित्र को प्रस्तुत करते रहे।
यह मनोज कुमार के लिए स्मृतिलेख नहीं है। यह लेख बताने की कोशिश करता है कि उन्होंने 1962 में चीन के साथ लड़ाई से लेकर 1975 में इमरजेंसी तक के दौर में भारतीयों की दो पीढ़ियों के लिए देशभक्ति को परिभाषित करने में क्या भूमिका निभाई।
यह उन्होंने ‘भारत’ के रूप में त्यागी, वीर और हमेशा विजयी होने वाले पात्र की भूमिका निभाकर किया- 1967 में ‘उपकार’ में एक आम सैनिक (और हरियाणा के किसान के बेटे) की; 1969 में ‘पूरब और पश्चिम’ में धोखा खाए स्वतंत्रता सेनानी के बेटे की; 1974 में ‘रोटी, कपड़ा और मकान’ में एक बेरोजगार इंजीनियर की भूमिकाएं निभाकर।
इनमें से हर फिल्म ने इंदिरा युग के प्रारंभिक दौर से लेकर तेजी से बदलते भारत की तस्वीर पेश की, जिसका सिलसिला इमरजेंसी लगाए जाने के साथ टूट गया और इसके बाद ‘एंग्री यंगमैन’ का युग शुरू हो गया। हम सब जानते हैं कि इसकी मशाल अमिताभ बच्चन ने कैसे थाम ली थी।
मनोज कुमार 1965 की फिल्म ‘शहीद’ में भगत सिंह बने। यह फिल्म हिट हुई और उनका सितारा बुलंद हुआ। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह फिल्म देखी थी और शास्त्री ने उनसे कहा था कि ‘आप जय जवान, जय किसान की थीम पर फिल्म क्यों नहीं बनाते।’ और जल्द ही, 1967 में मनोज कुमार ने ‘उपकार’ बनाई। फिल्म का हीरो एक किसान है, जो फौजी के रूप में 1965 की लड़ाई लड़ता है।
‘भारत’ नाम के किरदार को मनोज कुमार ने 1969 की फिल्म ‘पूरब और पश्चिम’ में एक अलग ही कहानी के साथ पेश किया। आज जब ‘इंडिया’ की जगह भारत पर जोर दिया जा रहा है, तब यह फिल्म बनी होती तो न केवल इसे ‘टैक्स फ्री’ किया जाता बल्कि प्रधानमंत्री, उनका पूरा मंत्रिमंडल, सभी मुख्यमंत्री और सरसंघचालक तक इसे देखने आते।
‘उपकार’ से अलग, इस फिल्म की कहानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के इर्द-गिर्द बुनी गई है। धोखा खाए (और कत्ल किए गए) स्वतंत्रता सेनानी का बेटा लंदन पहुंचता है। लेकिन परिवार के मित्र की जिस बेटी (सायरा बानो) के साथ उसका रिश्ता जुड़ने वाला है, वह पश्चिमी रंग-ढंग में इतनी रंगी है कि सिगरेट-शराब पीती है, भूरे बालों वाला विग पहनती है और वह तो क्या उसके पिता या हिप्पी भाई न तो कभी भारत गए और न इसकी कोई परवाह करते हैं।
उस पीढ़ी के ‘एनआरआई’ भारत के नाम से नाक-भौं सिकोड़ते थे, लेकिन ‘भारत’ नाम का हीरो उन्हें समझाने में जुट जाता है। इस कोशिश में वह ‘जब जीरो दिया मेरे भारत ने…’ गाना भी गाता है, जब कोई उस पर ताना कसता है कि भारत ने दुनिया को दिया क्या? इस फिल्म ने उन सुपरहिट फिल्मों के बीच भी अपना परचम लहराए रखा, जिनसे उस मेगास्टार (राजेश खन्ना) का जन्म हुआ, जो कई पीढ़ियों तक छाया रहा।
उनकी फिल्म ने ‘एनआरआई’ का मखौल उड़ाया, मगर लंदन में वह लगातार 50 हफ्तों तक चली थी। 1965 के बाद के फौजी माहौल वाले वर्षों के बाद भारत की चिंताएं जीवन, बेरोजगारी, भूख, घूसखोरी, भ्रष्टाचार जैसे मसलों के इर्द-गिर्द केंद्रित हो गईं। इसलिए ‘रोटी, कपड़ा और मकान’ में नए ‘भारत’ ने अवतार लिया।
यह उस योग्य इंजीनियर की कहानी कहती है, जो इतना ईमानदार है कि नौकरी नहीं खोज पाता और न नौकरी में टिक पाता है, वह अपनी गर्लफ्रेंड जीनत अमान के साथ ‘आकाशवाणी’ पर गाने गाकर किसी तरह गुजर-बसर करता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ अपने बॉस शशि कपूर के साथ चली जाती है। लेकिन ‘भारत’ संघर्ष करता है और विजयी होता है। ‘शोर’ की कहानी उसी साहसी, आम पीड़ित भारतीय की है, जो हड़ताल में अमीरों से संघर्ष करता है।
वे भारत के लिए अंधियारे, हताशा भरे साल थे। इंदिरा गांधी का समाजवाद तब मरणासन्न था। 1973 के बाद कच्चे तेल के झटकों ने रोजगारों पर कैंची चला दी थी और हमें राशन की दुकानों के आगे लाइन में खड़ा कर दिया था। मुद्रास्फीति की दर 30 फीसदी की ऊंचाई तक पहुंच गई थी।
बेरोजगारी उस दौर का प्रमुख मुद्दा था। गुलजार ने ‘मेरे अपने’ में इस मुद्दे को पहले ही उठाया था और मनोज कुमार ने भी इसे तुरंत पकड़ा था। वैसे, ‘रोटी, कपड़ा और मकान’ वाला मुहावरा भारतीय नहीं था। इसका आविष्कार शायद जु ल्फिकार अली भुट्टो ने किया था और वे ही इसका अक्सर इस्तेमाल करते थे।
इमरजेंसी ने मनोज कुमार की रफ्तार पर रोक लगा दी, लेकिन उन्होंने जिन सामाजिक-राजनीतिक हालात से संघर्ष किया, उसने ‘एंग्री यंगमैन’ को जन्म दिया। 80 के दशक में ‘समांतर सिनेमा’ आया। इस सिनेमा ने जातिवाद, पितृसत्ता और दूसरे अन्यायों से संघर्ष छेड़ दिया।
राष्ट्रवाद ने तमिल सिनेमा के जरिए वापसी की। ‘रोजा’ (1992) की कहानी कश्मीरी आतंकवादियों द्वारा इंडियन ऑइल के एक अधिकारी के अपहरण पर आधारित है। फिर सनी देओल का दौर भी आया। करगिल युद्ध ने अपनी तरह की फिल्मों को जन्म दिया, जिसकी अति चुनाव से पहले आई ‘उड़ी, द सर्जिकल स्ट्राइक’ से हुई। वैसे, सनी देओल की ‘बॉर्डर’ (1997) बेशक सबसे उत्प्रेरक फिल्म रही। मनोज कुमार के ‘भारत’ अगर आज होते तो क्या करते? ‘उपकार’ में तो उन्होंने युद्ध की बुराइयां गिनाई थीं, लेकिन आज उन्हें युद्ध जीतना ही होता।
बदलते भारत की तस्वीर पेश की थी “भारत’ कुमार ने मनोज कुमार की फिल्मों ने इंदिरा युग के प्रारंभिक दौर से लेकर तेजी से बदलते भारत की तस्वीर पेश की थी, जिसका सिलसिला 1975 में इमरजेंसी लगाए जाने के साथ टूट गया और इसके बाद ‘एंग्री यंगमैन’ का युग शुरू हो गया। (ये लेखक के अपने विचार हैं)
खबरें और भी हैं…
राजनीति की और खबर देखने के लिए यहाँ क्लिक करे – राजनीति
News
- Hindi News
- Opinion
- Shekhar Gupta’s Column How The Form Of Nationalism Changed On The Silver Screen
28 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
शेखर गुप्ता, एडिटर-इन-चीफ, ‘द प्रिन्ट’
पिछले छह दशकों में राष्ट्रभक्ति का विकास किस तरह हुआ, इसे समझने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि हम देखें भारतीय सिनेमा और खासकर बॉलीवुड ने अलग-अलग दौर में इसे कैसे परिभाषित किया। मनोज कुमार की मृत्यु हमें इस बात पर विचार करने का मौका देती है।
देशभक्ति, राष्ट्रवाद, नागरिक-बोध, अनुशासित जीवनशैली आदि सबको उन्होंने जितना परिभाषित किया, उतना किसी दूसरे अभिनेता ने शायद ही किया होगा। अपने पसंदीदा नाम ‘भारत’ के रूप में वे तरह-तरह के किरदारों को फिल्मी परदे पर जीते हुए एक मुकम्मल भारतीय के चरित्र को प्रस्तुत करते रहे।
यह मनोज कुमार के लिए स्मृतिलेख नहीं है। यह लेख बताने की कोशिश करता है कि उन्होंने 1962 में चीन के साथ लड़ाई से लेकर 1975 में इमरजेंसी तक के दौर में भारतीयों की दो पीढ़ियों के लिए देशभक्ति को परिभाषित करने में क्या भूमिका निभाई।
यह उन्होंने ‘भारत’ के रूप में त्यागी, वीर और हमेशा विजयी होने वाले पात्र की भूमिका निभाकर किया- 1967 में ‘उपकार’ में एक आम सैनिक (और हरियाणा के किसान के बेटे) की; 1969 में ‘पूरब और पश्चिम’ में धोखा खाए स्वतंत्रता सेनानी के बेटे की; 1974 में ‘रोटी, कपड़ा और मकान’ में एक बेरोजगार इंजीनियर की भूमिकाएं निभाकर।
इनमें से हर फिल्म ने इंदिरा युग के प्रारंभिक दौर से लेकर तेजी से बदलते भारत की तस्वीर पेश की, जिसका सिलसिला इमरजेंसी लगाए जाने के साथ टूट गया और इसके बाद ‘एंग्री यंगमैन’ का युग शुरू हो गया। हम सब जानते हैं कि इसकी मशाल अमिताभ बच्चन ने कैसे थाम ली थी।
मनोज कुमार 1965 की फिल्म ‘शहीद’ में भगत सिंह बने। यह फिल्म हिट हुई और उनका सितारा बुलंद हुआ। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह फिल्म देखी थी और शास्त्री ने उनसे कहा था कि ‘आप जय जवान, जय किसान की थीम पर फिल्म क्यों नहीं बनाते।’ और जल्द ही, 1967 में मनोज कुमार ने ‘उपकार’ बनाई। फिल्म का हीरो एक किसान है, जो फौजी के रूप में 1965 की लड़ाई लड़ता है।
‘भारत’ नाम के किरदार को मनोज कुमार ने 1969 की फिल्म ‘पूरब और पश्चिम’ में एक अलग ही कहानी के साथ पेश किया। आज जब ‘इंडिया’ की जगह भारत पर जोर दिया जा रहा है, तब यह फिल्म बनी होती तो न केवल इसे ‘टैक्स फ्री’ किया जाता बल्कि प्रधानमंत्री, उनका पूरा मंत्रिमंडल, सभी मुख्यमंत्री और सरसंघचालक तक इसे देखने आते।
‘उपकार’ से अलग, इस फिल्म की कहानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के इर्द-गिर्द बुनी गई है। धोखा खाए (और कत्ल किए गए) स्वतंत्रता सेनानी का बेटा लंदन पहुंचता है। लेकिन परिवार के मित्र की जिस बेटी (सायरा बानो) के साथ उसका रिश्ता जुड़ने वाला है, वह पश्चिमी रंग-ढंग में इतनी रंगी है कि सिगरेट-शराब पीती है, भूरे बालों वाला विग पहनती है और वह तो क्या उसके पिता या हिप्पी भाई न तो कभी भारत गए और न इसकी कोई परवाह करते हैं।
उस पीढ़ी के ‘एनआरआई’ भारत के नाम से नाक-भौं सिकोड़ते थे, लेकिन ‘भारत’ नाम का हीरो उन्हें समझाने में जुट जाता है। इस कोशिश में वह ‘जब जीरो दिया मेरे भारत ने…’ गाना भी गाता है, जब कोई उस पर ताना कसता है कि भारत ने दुनिया को दिया क्या? इस फिल्म ने उन सुपरहिट फिल्मों के बीच भी अपना परचम लहराए रखा, जिनसे उस मेगास्टार (राजेश खन्ना) का जन्म हुआ, जो कई पीढ़ियों तक छाया रहा।
उनकी फिल्म ने ‘एनआरआई’ का मखौल उड़ाया, मगर लंदन में वह लगातार 50 हफ्तों तक चली थी। 1965 के बाद के फौजी माहौल वाले वर्षों के बाद भारत की चिंताएं जीवन, बेरोजगारी, भूख, घूसखोरी, भ्रष्टाचार जैसे मसलों के इर्द-गिर्द केंद्रित हो गईं। इसलिए ‘रोटी, कपड़ा और मकान’ में नए ‘भारत’ ने अवतार लिया।
यह उस योग्य इंजीनियर की कहानी कहती है, जो इतना ईमानदार है कि नौकरी नहीं खोज पाता और न नौकरी में टिक पाता है, वह अपनी गर्लफ्रेंड जीनत अमान के साथ ‘आकाशवाणी’ पर गाने गाकर किसी तरह गुजर-बसर करता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ अपने बॉस शशि कपूर के साथ चली जाती है। लेकिन ‘भारत’ संघर्ष करता है और विजयी होता है। ‘शोर’ की कहानी उसी साहसी, आम पीड़ित भारतीय की है, जो हड़ताल में अमीरों से संघर्ष करता है।
वे भारत के लिए अंधियारे, हताशा भरे साल थे। इंदिरा गांधी का समाजवाद तब मरणासन्न था। 1973 के बाद कच्चे तेल के झटकों ने रोजगारों पर कैंची चला दी थी और हमें राशन की दुकानों के आगे लाइन में खड़ा कर दिया था। मुद्रास्फीति की दर 30 फीसदी की ऊंचाई तक पहुंच गई थी।
बेरोजगारी उस दौर का प्रमुख मुद्दा था। गुलजार ने ‘मेरे अपने’ में इस मुद्दे को पहले ही उठाया था और मनोज कुमार ने भी इसे तुरंत पकड़ा था। वैसे, ‘रोटी, कपड़ा और मकान’ वाला मुहावरा भारतीय नहीं था। इसका आविष्कार शायद जु ल्फिकार अली भुट्टो ने किया था और वे ही इसका अक्सर इस्तेमाल करते थे।
इमरजेंसी ने मनोज कुमार की रफ्तार पर रोक लगा दी, लेकिन उन्होंने जिन सामाजिक-राजनीतिक हालात से संघर्ष किया, उसने ‘एंग्री यंगमैन’ को जन्म दिया। 80 के दशक में ‘समांतर सिनेमा’ आया। इस सिनेमा ने जातिवाद, पितृसत्ता और दूसरे अन्यायों से संघर्ष छेड़ दिया।
राष्ट्रवाद ने तमिल सिनेमा के जरिए वापसी की। ‘रोजा’ (1992) की कहानी कश्मीरी आतंकवादियों द्वारा इंडियन ऑइल के एक अधिकारी के अपहरण पर आधारित है। फिर सनी देओल का दौर भी आया। करगिल युद्ध ने अपनी तरह की फिल्मों को जन्म दिया, जिसकी अति चुनाव से पहले आई ‘उड़ी, द सर्जिकल स्ट्राइक’ से हुई। वैसे, सनी देओल की ‘बॉर्डर’ (1997) बेशक सबसे उत्प्रेरक फिल्म रही। मनोज कुमार के ‘भारत’ अगर आज होते तो क्या करते? ‘उपकार’ में तो उन्होंने युद्ध की बुराइयां गिनाई थीं, लेकिन आज उन्हें युद्ध जीतना ही होता।
बदलते भारत की तस्वीर पेश की थी “भारत’ कुमार ने मनोज कुमार की फिल्मों ने इंदिरा युग के प्रारंभिक दौर से लेकर तेजी से बदलते भारत की तस्वीर पेश की थी, जिसका सिलसिला 1975 में इमरजेंसी लगाए जाने के साथ टूट गया और इसके बाद ‘एंग्री यंगमैन’ का युग शुरू हो गया। (ये लेखक के अपने विचार हैं)
News