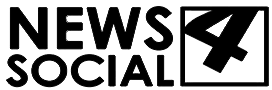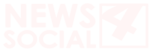मोंटेक सिंह अहलूवालिया का कॉलम: जलवायु संकट के साथ ही बढ़ रही हैं फंडिंग की जरूरतें
- Hindi News
- Opinion
- Montek Singh Ahluwalia’s Column Funding Needs Are Increasing With The Climate Crisis
5 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
मोंटेक सिंह अहलूवालिया
पिछले साल बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी29) में विकसित देशों ने, विकासशील देशों में जलवायु के लिए सालाना 300 अरब डॉलर जुटाने पर सहमति जताई थी। भले ही यह आंकड़ा पिछले लक्ष्य से तीन गुना अधिक है, लेकिन यह जलवायु के लिए जरूरी वित्त की कमी पूरी करने के लिए बहुत कम है।
आज की चुनौती 2015 में पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के समय से कहीं जटिल है। उस समय 100 अरब डॉलर का आंकड़ा वास्तविक निवेश आवश्यकताओं का विश्लेषण किए बिना तय किया गया था। इसके विपरीत सीओपी29 को वास्तविक लागतों का अनुमान लगाना था।
मैं जलवायु वित्त पर स्वतंत्र उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समूह (आईएचएलईजी) का सदस्य हूं। इसकी एक रिपोर्ट में पाया गया है कि विकासशील देशों (चीन को छोड़कर) को 2035 तक 2.4-3.3 ट्रिलियन डॉलर के जलवायु वित्त की जरूरत होगी।
इसका लगभग 60% हिस्सा बचत बढ़ाकर और सार्वजनिक घाटे को कम करके घरेलू स्तर पर हासिल किया जा सकता है। फिर भी 2030 तक 1 और 2035 तक 1.3 ट्रिलियन डॉलर की कमी बनी रहेगी। इस अंतर को पाटने के लिए बाहरी वित्तपोषण जरूरी है।
सीओपी29 में वित्तपोषण की कमी को तो स्वीकार किया गया, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बन पाई थी कि इसकी पूर्ति कैसे करें। विकासशील देशों ने इस पर जोर दिया कि सार्वजनिक फंड की कमी को पूरा करने के लिए अमीर अर्थव्यवस्थाएं आगे आएं, जबकि विकसित देशों ने सालाना केवल 300 अरब डॉलर जुटाने की पेशकश की। साथ में एक शर्त भी जोड़ दी कि वे सीधे वित्त के प्रावधान की गारंटी नहीं दे रहे, बल्कि धन जुटाने में बस ‘अग्रणी भूमिका’ निभाएंगे।
आईएचएलईजी की रिपोर्ट बताती है कि 2035 तक 650 अरब डॉलर की फंडिंग की कमी को इक्विटी और ऋण सहित निजी निवेश से पूरा किया जा सकता है। लेकिन इससे एक गहरी खाई भी सामने आई। जहां विकसित देशों ने बजट पर दबाव को कम करने के लिए निजी पूंजी का पक्ष लिया, वहीं विकासशील देशों ने सार्वजनिक वित्तपोषण पर जोर दिया।
कई विकासशील देश निजी निवेश को आकर्षित करने में संघर्ष करते हैं, इसलिए वे अनुदान व ऋणों पर निर्भर रहते हैं। इन सार्वजनिक संसाधनों को कम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को देने का मतलब है कि मध्यम आय वाले देश निजी पूंजी पर और निर्भर हो जाएंगे।
आईएचएलईजी के अनुसार, जहां वर्ष 2022 में निजी जलवायु वित्त की आवश्यकता 40 अरब डॉलर थी, वहीं यह 2035 तक अनुमानित 650 अरब डॉलर हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर निवेश कुछ ही बाजारों में केंद्रित है, जिससे पहुंच असमान और अनिश्चित हो जाती है।
निजी पूंजी उपलब्ध होने पर भी, घरेलू नीतियों की वजह से निवेश को बढ़ावा नहीं मिलता है। कई सरकारें राजनीतिक कारणों से कृत्रिम रूप से ऊर्जा की कीमतें कम करती हैं, जिससे बिजली प्रदाता लाभ के साथ काम नहीं कर पाते। विदेशी निवेशक इसे जोखिम के रूप में देखते हैं और निवेश से हिचकते हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र का साथ अब भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी) और द्विपक्षीय संस्थाएं निजी निवेशकों के लिए जोखिम कम कर सकती हैं, साथ ही सरकारों को स्थिर और निवेश-अनुकूल वातावरण बनाने में मदद कर सकती हैं।
वैश्विक जलवायु प्रयासों के प्रति ट्रम्प प्रशासन का शत्रुतापूर्ण रवैया और जीवाश्म ईंधन के विस्तार पर उनका जोर अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त को कमजोर करेगा। ऐसे में क्या सालाना सीओपी बैठकें करना सही तरीका है?
हर साल हजारों अधिकारियों, बिजनेस लीडर्स और गैर सरकारी संगठनों को इकट्ठा करने से जरूरी है जलवायु संकट पर ध्यान केंद्रित करना और ऐसे निर्णय लेना, जिनके ठोस नतीजे निकलें। क्योंकि जलवायु संकट बढ़ रहा है।
यदि प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अपनी वास्तविक प्रतिबद्धताओं को टालती रहीं, तो भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के पास जलवायु वित्त वार्ता को जी20 या ब्रिक्स जैसे मंचों पर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। (© प्रोजेक्ट सिंडिकेट)
खबरें और भी हैं…
राजनीति की और खबर देखने के लिए यहाँ क्लिक करे – राजनीति
News
- Hindi News
- Opinion
- Montek Singh Ahluwalia’s Column Funding Needs Are Increasing With The Climate Crisis
5 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
मोंटेक सिंह अहलूवालिया
पिछले साल बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी29) में विकसित देशों ने, विकासशील देशों में जलवायु के लिए सालाना 300 अरब डॉलर जुटाने पर सहमति जताई थी। भले ही यह आंकड़ा पिछले लक्ष्य से तीन गुना अधिक है, लेकिन यह जलवायु के लिए जरूरी वित्त की कमी पूरी करने के लिए बहुत कम है।
आज की चुनौती 2015 में पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के समय से कहीं जटिल है। उस समय 100 अरब डॉलर का आंकड़ा वास्तविक निवेश आवश्यकताओं का विश्लेषण किए बिना तय किया गया था। इसके विपरीत सीओपी29 को वास्तविक लागतों का अनुमान लगाना था।
मैं जलवायु वित्त पर स्वतंत्र उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समूह (आईएचएलईजी) का सदस्य हूं। इसकी एक रिपोर्ट में पाया गया है कि विकासशील देशों (चीन को छोड़कर) को 2035 तक 2.4-3.3 ट्रिलियन डॉलर के जलवायु वित्त की जरूरत होगी।
इसका लगभग 60% हिस्सा बचत बढ़ाकर और सार्वजनिक घाटे को कम करके घरेलू स्तर पर हासिल किया जा सकता है। फिर भी 2030 तक 1 और 2035 तक 1.3 ट्रिलियन डॉलर की कमी बनी रहेगी। इस अंतर को पाटने के लिए बाहरी वित्तपोषण जरूरी है।
सीओपी29 में वित्तपोषण की कमी को तो स्वीकार किया गया, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बन पाई थी कि इसकी पूर्ति कैसे करें। विकासशील देशों ने इस पर जोर दिया कि सार्वजनिक फंड की कमी को पूरा करने के लिए अमीर अर्थव्यवस्थाएं आगे आएं, जबकि विकसित देशों ने सालाना केवल 300 अरब डॉलर जुटाने की पेशकश की। साथ में एक शर्त भी जोड़ दी कि वे सीधे वित्त के प्रावधान की गारंटी नहीं दे रहे, बल्कि धन जुटाने में बस ‘अग्रणी भूमिका’ निभाएंगे।
आईएचएलईजी की रिपोर्ट बताती है कि 2035 तक 650 अरब डॉलर की फंडिंग की कमी को इक्विटी और ऋण सहित निजी निवेश से पूरा किया जा सकता है। लेकिन इससे एक गहरी खाई भी सामने आई। जहां विकसित देशों ने बजट पर दबाव को कम करने के लिए निजी पूंजी का पक्ष लिया, वहीं विकासशील देशों ने सार्वजनिक वित्तपोषण पर जोर दिया।
कई विकासशील देश निजी निवेश को आकर्षित करने में संघर्ष करते हैं, इसलिए वे अनुदान व ऋणों पर निर्भर रहते हैं। इन सार्वजनिक संसाधनों को कम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को देने का मतलब है कि मध्यम आय वाले देश निजी पूंजी पर और निर्भर हो जाएंगे।
आईएचएलईजी के अनुसार, जहां वर्ष 2022 में निजी जलवायु वित्त की आवश्यकता 40 अरब डॉलर थी, वहीं यह 2035 तक अनुमानित 650 अरब डॉलर हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर निवेश कुछ ही बाजारों में केंद्रित है, जिससे पहुंच असमान और अनिश्चित हो जाती है।
निजी पूंजी उपलब्ध होने पर भी, घरेलू नीतियों की वजह से निवेश को बढ़ावा नहीं मिलता है। कई सरकारें राजनीतिक कारणों से कृत्रिम रूप से ऊर्जा की कीमतें कम करती हैं, जिससे बिजली प्रदाता लाभ के साथ काम नहीं कर पाते। विदेशी निवेशक इसे जोखिम के रूप में देखते हैं और निवेश से हिचकते हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र का साथ अब भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी) और द्विपक्षीय संस्थाएं निजी निवेशकों के लिए जोखिम कम कर सकती हैं, साथ ही सरकारों को स्थिर और निवेश-अनुकूल वातावरण बनाने में मदद कर सकती हैं।
वैश्विक जलवायु प्रयासों के प्रति ट्रम्प प्रशासन का शत्रुतापूर्ण रवैया और जीवाश्म ईंधन के विस्तार पर उनका जोर अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त को कमजोर करेगा। ऐसे में क्या सालाना सीओपी बैठकें करना सही तरीका है?
हर साल हजारों अधिकारियों, बिजनेस लीडर्स और गैर सरकारी संगठनों को इकट्ठा करने से जरूरी है जलवायु संकट पर ध्यान केंद्रित करना और ऐसे निर्णय लेना, जिनके ठोस नतीजे निकलें। क्योंकि जलवायु संकट बढ़ रहा है।
यदि प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अपनी वास्तविक प्रतिबद्धताओं को टालती रहीं, तो भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के पास जलवायु वित्त वार्ता को जी20 या ब्रिक्स जैसे मंचों पर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। (© प्रोजेक्ट सिंडिकेट)
News