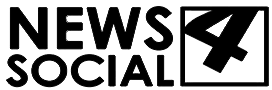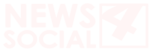जस्टिस मदन लोकुर का कॉलम: अगर समय पर न्याय चाहिए तो जजों की संख्या बढ़ानी होगी
- Hindi News
- Opinion
- Justice Madan Lokur’s Column If We Want Timely Justice, Then The Number Of Judges Will Have To Be Increased
8 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
जस्टिस मदन लोकुर सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति
आखिरकार भारत में कितने जज होने चाहिए? इस सवाल का जवाब कई बार दिया जा चुका है। 40 साल पहले, वर्ष 1987 में जब देश में औसत प्रति 10 लाख आबादी पर मात्र 10.5 जज थे, तब 120वें लॉ कमीशन ने समय पर न्याय दिलाना सुनिश्चित करने के लिए प्रति 10 लाख आबादी पर 50 जजों की सिफारिश की थी।
लेकिन आज भी देश में प्रति दस लाख लोगों पर 16 ही जज हैं और जजों की स्वीकृत संख्या लगभग 27 हजार है। कई राज्यों में जजों की स्वीकृत संख्या के एक-तिहाई पद खाली हैं। जजों की संख्या का सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि देश की अदालतों में आज 5 करोड़ से ज्यादा केस लंबित हैं। इनमें 4.5 करोड़ केस निचली अदालतों में ही हैं।
पेंडिंग केसों की बात करें तो 22 राज्यों की अधीनस्थ अदालतों में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 से 2025 तक 5 साल से अधिक समय से लंबित मामलों का प्रतिशत बढ़ा है। 2025 की रिपोर्ट का पूर्वानुमान कहता है कि निचली अदालतों और हाई कोर्ट में 2030 तक पेंडिंग केस 15% की दर से बढ़ेंगे। निचली अदालतों के लंबित केस वर्ष 2030 तक 5.12 करोड़ हो सकते हैं।
लंबित केसों का सीधा असर हर जज के कार्यभार पर पड़ता है। अलग-अलग राज्यों में 2024 के अंत तक प्रति जज औसत कार्यभार 2200 केस तक पहुंच गया था। कर्नाटक में प्रति जज लगभग 1,750 केस, केरल में 3,800 केस और उत्तर प्रदेश में 4,300 केसों का कार्यभार था। केवल सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यभार 300 केस प्रति जज से कम था।
ये मूलत: उच्च न्यायालयों की जिम्मेदारी है कि जजों के खाली पदों पर नियमित नियुक्ति हो और बढ़ते कार्यभार के अनुरूप जजों की निर्धारित संख्या भी बढ़ती रहे। लेकिन कई समितियों और कमीशंस की रिपोर्ट के बावजूद हालात जस के तस हैं। इसकी एक वजह वित्तीय संसाधनों की कमी बताई जाती है। जजों की संख्या बढ़ने के साथ ही उनके स्टाफ, कोर्टहॉल और जजों और उनके ज्युडिशियल स्टाफ के लिए आवास की भी जरूरत होती है।
जिला अदालतों में हर नए जज के लिए रजिस्ट्रार, स्टेनोग्राफर और दो क्लर्क समेत आठ का स्टाफ चाहिए। हालांकि, न्यायपालिका में निवेश से लाभ को समझना है तो न्यायिक प्रक्रिया में देरी के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को देखा जाना चाहिए।
इसलिए सरकारी धन को कम जरूरी या अनावश्यक जगहों के बजाय सही जगहों पर लगाना जरूरी है। जजों की संख्या बढ़ाने में चुनौती वित्तीय भार की ही नहीं है, बल्कि राज्य सरकारें और न्यायपालिका भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। दोनों ने कभी ऐसा स्पष्ट तरीका नहीं अपनाया जिससे पूरी व्यवस्था का वर्कफोर्स बढ़ता रहे।
जिला अदालतें हमारी न्याय व्यवस्था की रीढ़ रही हैं, लेकिन इसे मजबूत करने के लिए हमने क्या किया? अत्यधिक केसों के बोझ से दबे ज्यादातर जिला जजों को नए मामलों की तैयारी और उसमें दाखिल हुए दस्तावेजों को देखने, उनकी समीक्षा करने के लिए समय नहीं मिलता।
उदाहरण के लिए, अगर किसी नए आपराधिक केस में दर्जनों गवाह हैं तो जज महत्ता के आधार पर उनका अलग-अलग वर्गीकरण करना चाहेंगे। लेकिन अत्यधिक कार्यभार से दबे जजों के पास स्थगन और जल्दबाजी में आदेश देने जैसे अनुचित विकल्प बचते हैं, जिनमें न्यायिक विवेक की पर्याप्त झलक नहीं होती। वित्तीय मामलों से जुड़ी सुनवाई में और समय लगता है।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर, राज्य सरकारों या हाई कोर्ट की तरफ से देश के लगभग सभी 600 न्यायिक जिलों में कम से कम दो जजों के लिए एक-एक पेड ज्युडिशियल क्लर्क या रिसर्च एसोसिएट नियुक्त किए जा सकते हैं।
इनमें एक प्रधान जिला न्यायाधीश और दूसरे सबसे अधिक कार्यभार वाले जज हों। हर क्लर्क को 25,000 रुपए भी दिए जाएं तो 600 न्यायिक जिलों में 1,200 ज्युडिशियल क्लर्क पर सालाना 36 करोड़ रुपए से अधिक खर्च नहीं होंगे। लेकिन इससे मुकदमे जल्दी निपटने, अधिक गुणवत्तापूर्ण फैसले और समय पर न्याय मिलने जैसे फायदे होंगे। (ये लेखक के अपने विचार हैं। इस लेख के सहलेखक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के सह-संस्थापक वलय सिंह हैं।)
खबरें और भी हैं…
राजनीति की और खबर देखने के लिए यहाँ क्लिक करे – राजनीति
News
- Hindi News
- Opinion
- Justice Madan Lokur’s Column If We Want Timely Justice, Then The Number Of Judges Will Have To Be Increased
8 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
जस्टिस मदन लोकुर सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति
आखिरकार भारत में कितने जज होने चाहिए? इस सवाल का जवाब कई बार दिया जा चुका है। 40 साल पहले, वर्ष 1987 में जब देश में औसत प्रति 10 लाख आबादी पर मात्र 10.5 जज थे, तब 120वें लॉ कमीशन ने समय पर न्याय दिलाना सुनिश्चित करने के लिए प्रति 10 लाख आबादी पर 50 जजों की सिफारिश की थी।
लेकिन आज भी देश में प्रति दस लाख लोगों पर 16 ही जज हैं और जजों की स्वीकृत संख्या लगभग 27 हजार है। कई राज्यों में जजों की स्वीकृत संख्या के एक-तिहाई पद खाली हैं। जजों की संख्या का सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि देश की अदालतों में आज 5 करोड़ से ज्यादा केस लंबित हैं। इनमें 4.5 करोड़ केस निचली अदालतों में ही हैं।
पेंडिंग केसों की बात करें तो 22 राज्यों की अधीनस्थ अदालतों में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 से 2025 तक 5 साल से अधिक समय से लंबित मामलों का प्रतिशत बढ़ा है। 2025 की रिपोर्ट का पूर्वानुमान कहता है कि निचली अदालतों और हाई कोर्ट में 2030 तक पेंडिंग केस 15% की दर से बढ़ेंगे। निचली अदालतों के लंबित केस वर्ष 2030 तक 5.12 करोड़ हो सकते हैं।
लंबित केसों का सीधा असर हर जज के कार्यभार पर पड़ता है। अलग-अलग राज्यों में 2024 के अंत तक प्रति जज औसत कार्यभार 2200 केस तक पहुंच गया था। कर्नाटक में प्रति जज लगभग 1,750 केस, केरल में 3,800 केस और उत्तर प्रदेश में 4,300 केसों का कार्यभार था। केवल सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यभार 300 केस प्रति जज से कम था।
ये मूलत: उच्च न्यायालयों की जिम्मेदारी है कि जजों के खाली पदों पर नियमित नियुक्ति हो और बढ़ते कार्यभार के अनुरूप जजों की निर्धारित संख्या भी बढ़ती रहे। लेकिन कई समितियों और कमीशंस की रिपोर्ट के बावजूद हालात जस के तस हैं। इसकी एक वजह वित्तीय संसाधनों की कमी बताई जाती है। जजों की संख्या बढ़ने के साथ ही उनके स्टाफ, कोर्टहॉल और जजों और उनके ज्युडिशियल स्टाफ के लिए आवास की भी जरूरत होती है।
जिला अदालतों में हर नए जज के लिए रजिस्ट्रार, स्टेनोग्राफर और दो क्लर्क समेत आठ का स्टाफ चाहिए। हालांकि, न्यायपालिका में निवेश से लाभ को समझना है तो न्यायिक प्रक्रिया में देरी के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को देखा जाना चाहिए।
इसलिए सरकारी धन को कम जरूरी या अनावश्यक जगहों के बजाय सही जगहों पर लगाना जरूरी है। जजों की संख्या बढ़ाने में चुनौती वित्तीय भार की ही नहीं है, बल्कि राज्य सरकारें और न्यायपालिका भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। दोनों ने कभी ऐसा स्पष्ट तरीका नहीं अपनाया जिससे पूरी व्यवस्था का वर्कफोर्स बढ़ता रहे।
जिला अदालतें हमारी न्याय व्यवस्था की रीढ़ रही हैं, लेकिन इसे मजबूत करने के लिए हमने क्या किया? अत्यधिक केसों के बोझ से दबे ज्यादातर जिला जजों को नए मामलों की तैयारी और उसमें दाखिल हुए दस्तावेजों को देखने, उनकी समीक्षा करने के लिए समय नहीं मिलता।
उदाहरण के लिए, अगर किसी नए आपराधिक केस में दर्जनों गवाह हैं तो जज महत्ता के आधार पर उनका अलग-अलग वर्गीकरण करना चाहेंगे। लेकिन अत्यधिक कार्यभार से दबे जजों के पास स्थगन और जल्दबाजी में आदेश देने जैसे अनुचित विकल्प बचते हैं, जिनमें न्यायिक विवेक की पर्याप्त झलक नहीं होती। वित्तीय मामलों से जुड़ी सुनवाई में और समय लगता है।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर, राज्य सरकारों या हाई कोर्ट की तरफ से देश के लगभग सभी 600 न्यायिक जिलों में कम से कम दो जजों के लिए एक-एक पेड ज्युडिशियल क्लर्क या रिसर्च एसोसिएट नियुक्त किए जा सकते हैं।
इनमें एक प्रधान जिला न्यायाधीश और दूसरे सबसे अधिक कार्यभार वाले जज हों। हर क्लर्क को 25,000 रुपए भी दिए जाएं तो 600 न्यायिक जिलों में 1,200 ज्युडिशियल क्लर्क पर सालाना 36 करोड़ रुपए से अधिक खर्च नहीं होंगे। लेकिन इससे मुकदमे जल्दी निपटने, अधिक गुणवत्तापूर्ण फैसले और समय पर न्याय मिलने जैसे फायदे होंगे। (ये लेखक के अपने विचार हैं। इस लेख के सहलेखक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के सह-संस्थापक वलय सिंह हैं।)
News