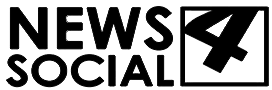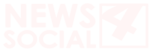कौशिक बसु का कॉ़लम: ट्रम्प ने अपने पैरों पर टैरिफ की कुल्हाड़ी मार ली है
- Hindi News
- Opinion
- Kaushik Basu’s Column Trump Has Shot Himself In The Foot With Tariffs
7 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
कौशिक बसु विश्व बैंक के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट
अमेरिका के द्वारा आयात की जाने वाली सभी कारों और लाइट-ड्यूटी ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाने वाले ट्रम्प के कार्यकारी आदेश 3 अप्रैल से प्रभावी हो गए। यह अमेरिका द्वारा अपने व्यापारिक साझेदारों पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने के एक दिन बाद हुआ। हालांकि ट्रम्प ने घबराए हुए अमेरिकियों को यह कहकर आश्वस्त करने की कोशिश की कि हमारा ऑटोमोबाइल व्यवसाय पहले की तरह फलेगा-फूलेगा।
सच्चाई यह है कि ऐसा नहीं होगा। जहां ट्रम्प के टैरिफ पारंपरिक आर्थिक सूझबूझ- एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो से लेकर जॉन मेनार्ड कीन्स और मिल्टन फ्रीडमैन तक- को ताक पर रखने वाले हैं, वहीं उनका अति-आत्मविश्वास कुछ लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि इसके पीछे कोई छिपा हुआ तर्क जरूर होगा।
संभवतः, कारों और ट्रकों पर टैरिफ लगाने का मकसद ऑटोमेकर्स को अमेरिका में कारखाने लगाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। लेकिन बारीकी से मुआयना करने पर साफ होता है कि यह तर्क दोषपूर्ण है। और जहां यह कई देशों- विशेष रूप से कनाडा, मैक्सिको और जापान पर नकारात्मक असर डालेगा, वहीं सबसे बुरी मार तो अमेरिका पर ही पड़ेगी।
टैरिफ से अमेरिका में कारों की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन यह तो केवल एक ही पहलू है। ऑटोमोबाइल और सेमीकंडक्टर जैसे उद्योगों की एक निश्चित उत्पादन लागत होती है। भूमि अधिग्रहण, कारखाने और परमिट में आने वाली निश्चित लागतों के बाद अचानक टैरिफ में कमी से काफी नुकसान हो सकता है।
ऐसे में निवेशकों को यह आश्वासन देने की आवश्यकता होगी कि टैरिफ कम से कम 10-15 वर्षों तक लागू रहेंगे। तभी इस बात की संभावना है कि अमेरिका में नई कार फैक्टरियां स्थापित होंगी, जिससे श्रम की मांग बढ़ेगी।
लेकिन अमेरिकी ऑटोमोबाइल को फिर से ‘ग्रेट’ बनाने के उलट, पारंपरिक श्रम की मांग में कृत्रिम वृद्धि अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। अमेरिकी बाजार के टैरिफ की दीवार के पीछे सुरक्षित होने से घरेलू उत्पादन तेजी से महंगा होता चला जाएगा।
इससे चीन, भारत, मैक्सिको और इंडोनेशिया जैसे स्वाभाविक रूप से कम श्रम-लागत वाले देश बहुत कम कीमतों पर कारों का उत्पादन करने में सक्षम होंगे। वे अमेरिका से आगे निकल जाएंगे और वैश्विक बाजार में मजबूती से पैर जमा लेंगे।
ऑटो मैन्युफैक्चरिंग को वापस लाने के लिए ट्रम्प के प्रयास अमेरिका द्वारा अपने कपड़ा उद्योग में गिरावट को संभालने के तरीके से बिल्कुल अलग हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका कपड़ा उद्योग में अग्रणी था और वहां कपास और ऊन की मिलें पूरी क्षमता से चल रही थीं। लेकिन जैसे-जैसे अमेरिका अमीर होता गया और श्रम लागत बढ़ती गई, उसने अपना तुलनात्मक लाभ खो दिया और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया, जिनमें रिसर्च और इनोवेशन की आवश्यकता थी। वह इन क्षेत्रों में नेतृत्व करने के लिए अच्छी स्थिति में था। वहीं कपड़ा उद्योग पर वियतनाम, बांग्लादेश और तुर्किये जैसे देशों का दबदबा हो गया।
अगर अमेरिका ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए 20वीं सदी के उत्तरार्ध में आयातित वस्त्रों और परिधानों पर भारी टैरिफ लगाने का फैसला किया होता, तो वह शायद गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बना रहता। लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती : अमेरिकी अर्थव्यवस्था आज जिस मुकाम पर है, वहां नहीं होती। इसके बजाय, उसके पास बड़ी-बड़ी फैक्टरियां होतीं, जहां कर्मचारी लेबर-इंटेंसिव नौकरियों में काम करते।
इसका मतलब यह नहीं है कि टैरिफ प्रभावी नहीं होते। लेकिन जब वे किसी देश की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को कमजोर करते हैं- जैसा कि ट्रम्प के टैरिफ करेंगे- तो वे केवल नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। धुर-राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद के खिलाफ इतिहास हमें सचेत करता है।
20वीं सदी की शुरुआत में अर्जेंटीना तेजी से बढ़ रहा था और जर्मनी और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बन गया था। लेकिन 1930 में सब बदल गया, जब खोसे फीलिक्स उरीबुरू ने सैन्य तख्तापलट करके खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया।
तीन साल के भीतर ही उन्होंने इमिग्रेशन पर रोक लगा दी और टैरिफ को लगभग दोगुना कर दिया। दूसरी तरफ, अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को लगातार खोल रहा था, उच्च शिक्षा में निवेश कर रहा था और अत्याधुनिक शोध कर रहा था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उछाल आया जबकि अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रही और धीरे-धीरे उसने अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने की तमाम क्षमताएं गंवा दीं।
अमेरिकी बाजार के टैरिफ की दीवार के पीछे सुरक्षित होने से घरेलू उत्पादन महंगा होता चला जाएगा। इससे भारत जैसे कम श्रम-लागत वाले देश कम कीमतों पर कारों का उत्पादन करने में सक्षम होंगे और अमेरिका से आगे निकल जाएंगे।
(© प्रोजेक्ट सिंडिकेट)
खबरें और भी हैं…
राजनीति की और खबर देखने के लिए यहाँ क्लिक करे – राजनीति
News
- Hindi News
- Opinion
- Kaushik Basu’s Column Trump Has Shot Himself In The Foot With Tariffs
7 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
कौशिक बसु विश्व बैंक के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट
अमेरिका के द्वारा आयात की जाने वाली सभी कारों और लाइट-ड्यूटी ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाने वाले ट्रम्प के कार्यकारी आदेश 3 अप्रैल से प्रभावी हो गए। यह अमेरिका द्वारा अपने व्यापारिक साझेदारों पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने के एक दिन बाद हुआ। हालांकि ट्रम्प ने घबराए हुए अमेरिकियों को यह कहकर आश्वस्त करने की कोशिश की कि हमारा ऑटोमोबाइल व्यवसाय पहले की तरह फलेगा-फूलेगा।
सच्चाई यह है कि ऐसा नहीं होगा। जहां ट्रम्प के टैरिफ पारंपरिक आर्थिक सूझबूझ- एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो से लेकर जॉन मेनार्ड कीन्स और मिल्टन फ्रीडमैन तक- को ताक पर रखने वाले हैं, वहीं उनका अति-आत्मविश्वास कुछ लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि इसके पीछे कोई छिपा हुआ तर्क जरूर होगा।
संभवतः, कारों और ट्रकों पर टैरिफ लगाने का मकसद ऑटोमेकर्स को अमेरिका में कारखाने लगाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। लेकिन बारीकी से मुआयना करने पर साफ होता है कि यह तर्क दोषपूर्ण है। और जहां यह कई देशों- विशेष रूप से कनाडा, मैक्सिको और जापान पर नकारात्मक असर डालेगा, वहीं सबसे बुरी मार तो अमेरिका पर ही पड़ेगी।
टैरिफ से अमेरिका में कारों की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन यह तो केवल एक ही पहलू है। ऑटोमोबाइल और सेमीकंडक्टर जैसे उद्योगों की एक निश्चित उत्पादन लागत होती है। भूमि अधिग्रहण, कारखाने और परमिट में आने वाली निश्चित लागतों के बाद अचानक टैरिफ में कमी से काफी नुकसान हो सकता है।
ऐसे में निवेशकों को यह आश्वासन देने की आवश्यकता होगी कि टैरिफ कम से कम 10-15 वर्षों तक लागू रहेंगे। तभी इस बात की संभावना है कि अमेरिका में नई कार फैक्टरियां स्थापित होंगी, जिससे श्रम की मांग बढ़ेगी।
लेकिन अमेरिकी ऑटोमोबाइल को फिर से ‘ग्रेट’ बनाने के उलट, पारंपरिक श्रम की मांग में कृत्रिम वृद्धि अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। अमेरिकी बाजार के टैरिफ की दीवार के पीछे सुरक्षित होने से घरेलू उत्पादन तेजी से महंगा होता चला जाएगा।
इससे चीन, भारत, मैक्सिको और इंडोनेशिया जैसे स्वाभाविक रूप से कम श्रम-लागत वाले देश बहुत कम कीमतों पर कारों का उत्पादन करने में सक्षम होंगे। वे अमेरिका से आगे निकल जाएंगे और वैश्विक बाजार में मजबूती से पैर जमा लेंगे।
ऑटो मैन्युफैक्चरिंग को वापस लाने के लिए ट्रम्प के प्रयास अमेरिका द्वारा अपने कपड़ा उद्योग में गिरावट को संभालने के तरीके से बिल्कुल अलग हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका कपड़ा उद्योग में अग्रणी था और वहां कपास और ऊन की मिलें पूरी क्षमता से चल रही थीं। लेकिन जैसे-जैसे अमेरिका अमीर होता गया और श्रम लागत बढ़ती गई, उसने अपना तुलनात्मक लाभ खो दिया और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया, जिनमें रिसर्च और इनोवेशन की आवश्यकता थी। वह इन क्षेत्रों में नेतृत्व करने के लिए अच्छी स्थिति में था। वहीं कपड़ा उद्योग पर वियतनाम, बांग्लादेश और तुर्किये जैसे देशों का दबदबा हो गया।
अगर अमेरिका ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए 20वीं सदी के उत्तरार्ध में आयातित वस्त्रों और परिधानों पर भारी टैरिफ लगाने का फैसला किया होता, तो वह शायद गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बना रहता। लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती : अमेरिकी अर्थव्यवस्था आज जिस मुकाम पर है, वहां नहीं होती। इसके बजाय, उसके पास बड़ी-बड़ी फैक्टरियां होतीं, जहां कर्मचारी लेबर-इंटेंसिव नौकरियों में काम करते।
इसका मतलब यह नहीं है कि टैरिफ प्रभावी नहीं होते। लेकिन जब वे किसी देश की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को कमजोर करते हैं- जैसा कि ट्रम्प के टैरिफ करेंगे- तो वे केवल नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। धुर-राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद के खिलाफ इतिहास हमें सचेत करता है।
20वीं सदी की शुरुआत में अर्जेंटीना तेजी से बढ़ रहा था और जर्मनी और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बन गया था। लेकिन 1930 में सब बदल गया, जब खोसे फीलिक्स उरीबुरू ने सैन्य तख्तापलट करके खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया।
तीन साल के भीतर ही उन्होंने इमिग्रेशन पर रोक लगा दी और टैरिफ को लगभग दोगुना कर दिया। दूसरी तरफ, अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को लगातार खोल रहा था, उच्च शिक्षा में निवेश कर रहा था और अत्याधुनिक शोध कर रहा था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उछाल आया जबकि अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रही और धीरे-धीरे उसने अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने की तमाम क्षमताएं गंवा दीं।
अमेरिकी बाजार के टैरिफ की दीवार के पीछे सुरक्षित होने से घरेलू उत्पादन महंगा होता चला जाएगा। इससे भारत जैसे कम श्रम-लागत वाले देश कम कीमतों पर कारों का उत्पादन करने में सक्षम होंगे और अमेरिका से आगे निकल जाएंगे।
(© प्रोजेक्ट सिंडिकेट)
News